"फ़िल्म: पर्दे तक सीमित एक कहानी"
●●●
फिल्मों में जो अति-काल्पनिक दिखावे का आजकल चलन चला है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे दर्शक 'मनोरंजन' नामक डिवाइस के ज़रिए कितनी आसानी से कैच करते हुए मिल जाते हैं। वैसे एक बात तो है, फ़िल्मों में किसी विलन का क़िरदार माशाल्लाह! बहुत कमाल होता है। आज सुबह ही अमिताभ की फ़िल्म 'शहंशाह' देख रहा था। फाइटिंग के एक सीन में इस फ़ौलादी हीरो को पीटने अथाह गुंडे आ जाते हैं। कुछ एकदम मुश्टण्डे, कुछ काले-कूबरे, कुछ सूखे-पाखे, कुछ कद्दू सा पेट लिए, कुछ पिचके मुँह के और कुछ उजड़े चमन एकदम कडुआ तेल लगाकर चिकनी खोपड़ी लेकर आये। सूरज की किरणों से चमकते ये टकले समाज भर में निकम्मेपन का 'फॉक्स' मारते फिरते हैं। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था मानो ये सब किसी की बारात में नाचने के लिए भाड़े पर मँगवाये गए हों। हक़ीक़त में इन्हें ख़ुद पता नहीं होता कि थोड़ी देर में ये ही घोड़ी चढ़ाये जाएँगे। ऐसे में एक हमारा हीरो होता है, जो लाइट, कैमरा, एक्शन के तुरंत बाद ढेर सारे गुस्से और ताव में चिल्लाता है। जिसके चिल्लाने भर से गुंडों की पतलून गीली हो जाती है और जिस पर गुंडों की मार-कुटाई का कोई असर नहीं होता। उल्टा ये जनाब ही गुंडों का नाड़ा खोल देते हैं।
हमारे भारत की फ़िल्म इंडस्ट्रीज बहुत सोच समझकर विलन का क़िरदार वर्गीकृत करती है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। अधिकतर बॉलीवुड फ़िल्म में विलन का एक ही ढर्रा हमेशा से रहा है। वो यह कि या तो ये साहब किसी 'भौकाली' सरदार के नीचे काम करते हैं या तो किसी शरीफ़ और मलूक बिजनेसमैन के बिज़नेस में हाथ बटाते हैं। फिर एकदिन मौका पाते ही अपने अन्नदाताओं को टपकाकर एक ही घिसा-पिटा डायलॉग बोलते हुए मिल जाते हैं कि 'इस दिन का मैंने बरसों इंतज़ार किया है, तब जाकर आज मेरा सपना पूरा हुआ।' अब इनसे कहो कि अबे उल्लू के दिमाग़! इतने दिनों किसी गैराज में भी काम करता तो आज उसका मालिक तू होता भाई! ख़ैर, जाने दीजिए। तिसपर हीरो, हीरो का तो क्या ही कहें, आज के दौर में अकेला ही पूरे देश को निपटाने की सामर्थ्य रखता है।
दूसरा सबसे मशहूर टॉलीवुड इंडस्ट्रीज का नंबर आता है साहब! यहाँ मेन विलन से एक पोस्ट नीचे वाले गुर्गे ने सांडनुमा शरीर और कोयला खदान की आग में भुने हुए भक्क काले टट्टू पाल रखे होते हैं। जिनके हाथों में भगवान परशुराम के फरशे, असुर सम्राट रावण की तलवार से लेकर नारियल छीलने वाले भारी-भरकम चाकू की मौज़ूदगी होती है। मेन विलन की भूमिका में प्रकाश राज, आशीष विद्यार्थी, प्रदीप रावत, रघुवरन, जगपति बाबू और सोनू सूद जैसे हेकड़ और चौखड़ पट्ठे सामने निकल कर आते हैं। ये फ़िल्मों में अधिकतर रंजिश को भुनाते और भूनते हुए मिल जाते हैं या फिर इनकी लड़की का प्रेम प्रसंग उस हीरो से होते हुए चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका होता है जो जाने-अनजाने उस 'विलन' के लिए 'विलन' का रोल ही प्ले करता है।
मार-कुटाई के सीन में जब हीरो इन टट्टुओं की कुटाई करता है, तब किसी के मुँह के आगे इनके जूते का सोल पंखे से भी तेज हवा फेंकने लगता है। हीरो के एक घूँसे में सात समंदर पार की सुखद यात्रा का अनुभव भी इन टट्टुओं को ही नसीब होता है। हीरो वह महान व्यक्ति है जो अपनी माँ समान मिट्टी से प्रेम न करने वाले चिलगोजों को नाक रगड़ते हुए भूमि वंदन करने की विधि सिखाने की हैसियत रखता है। मतलब! सौ-सौ गुंडे एक सूखे-पाखे धनुष जैसे हीरो का जब कुछ नहीं उखाड़ पाते तो सिक्स पैक एब्स वालों का कुछ भी बिगाड़ पाना नामुमकिन ही होता है।
एक और बात, जो इन सारी फिल्मों में दिलचस्प होती है, वो यह कि जितना ताक़तवर विलन, उतना ही ताक़तवर हीरो। हीरो भाईसाहब को विलन मोटी-मोटी लोहे की रॉड से कितना भी मार ले पर साहब टस से मस नहीं होते बल्कि आँखों से इशारा देते हैं कि 'लल्लू! तू तो गया काम से।' विलन की नापाक हरक़त का हासिल सिर्फ़ इतना होता है कि हीरो उठकर खड़ा हो जाता है जिसे देखते ही घंटों से हीरो की कुटाई कर रहे विलन को मिली थकान और बौखलाहट के मारे उसका चेहरा लाल-पीला हो जाता है। और यहाँ फिर कोई ग़लती होती है जिसके फलस्वरूप हीरो विलन को इतना लतियाता है कि जिसे देखकर भूत भी भाग जाए। अंत समय में विलन दुख भोगता हुआ नर्क के दरवाज़े पर अपनी नाक रगड़ता है और हीरो, अपनी हीरोइन या फिर फैमिली के साथ ख़ुश होते हुए फोटो खिंचा लेता है।
अब आते हैं लगभग तीन घंटे की फ़िल्म की असलियत पर। फ़िल्म ख़त्म होते ही दर्शकों का एक जत्था भक्तों की तरह खड़े होकर तालियाँ पीटता है जैसे रघुनाथ जी के दर्शन कर लिए हों और उनके आगे सिर झुका रहा हो। इसके अलावा थिएटर में बैठे आधे से ज़्यादा दर्शक दीर्घा में पड़े-पड़े ऊँघ रहे होते हैं। कभी-कभी कुछ एक दर्शक हीरो के मर जाने का ढेर सारा शोक मनाते हुए बाहर आते हैं और अपने दोस्तों की कमीज़ से ही नाक पोंछ कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे देते हैं। कभी मेरी पेशानी पर भी बल पड़ता था। सोचता था कि कैसे एक हीरो इतने गुंडों को मार लेता है? क्या हीरो इतना हैंडसम होता है? ये गुंडे काले-कूबरे और चौखटे जैसे मुँह के ही क्यों होते हैं? वगैरह, वगैरह। लेकिन जब बड़ा हुआ तो फ़िल्म देखते-देखते ही इन सब सवालों का जवाब भी मिल गया। फ़िलहाल, हम सबको अपने ज़ेहन में इस बात की गाँठ बाँधकर रखनी होगी कि मनोरंजन की दुनिया हक़ीक़त से कभी भी मेल नहीं खा सकती। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम अच्छाई को फिल्मों से निकालें और उन्हें आपने जीवन में आत्मसात करें। और हाँ! फ़िल्म देखने के दौरान नकारात्मकता और बनावटी पहलुओं को आग लगाकर मन के किसी भी कोने से दूर फेंक देना ही बेहतर होगा। अच्छा रहेगा कि हम तथ्यपरक और यथार्थ से जुड़ी फ़िल्मों को देखें। यह हमारे सुखद कल के लिए एकदम उपयुक्त चुनाव होगा वरना आने वाले परिणाम हमें अवश्य ही चिंतित करेंगे, जिस तरह से आज करते हैं।
-खेरवार
फिल्मों में जो अति-काल्पनिक दिखावे का आजकल चलन चला है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे दर्शक 'मनोरंजन' नामक डिवाइस के ज़रिए कितनी आसानी से कैच करते हुए मिल जाते हैं। वैसे एक बात तो है, फ़िल्मों में किसी विलन का क़िरदार माशाल्लाह! बहुत कमाल होता है। आज सुबह ही अमिताभ की फ़िल्म 'शहंशाह' देख रहा था। फाइटिंग के एक सीन में इस फ़ौलादी हीरो को पीटने अथाह गुंडे आ जाते हैं। कुछ एकदम मुश्टण्डे, कुछ काले-कूबरे, कुछ सूखे-पाखे, कुछ कद्दू सा पेट लिए, कुछ पिचके मुँह के और कुछ उजड़े चमन एकदम कडुआ तेल लगाकर चिकनी खोपड़ी लेकर आये। सूरज की किरणों से चमकते ये टकले समाज भर में निकम्मेपन का 'फॉक्स' मारते फिरते हैं। लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था मानो ये सब किसी की बारात में नाचने के लिए भाड़े पर मँगवाये गए हों। हक़ीक़त में इन्हें ख़ुद पता नहीं होता कि थोड़ी देर में ये ही घोड़ी चढ़ाये जाएँगे। ऐसे में एक हमारा हीरो होता है, जो लाइट, कैमरा, एक्शन के तुरंत बाद ढेर सारे गुस्से और ताव में चिल्लाता है। जिसके चिल्लाने भर से गुंडों की पतलून गीली हो जाती है और जिस पर गुंडों की मार-कुटाई का कोई असर नहीं होता। उल्टा ये जनाब ही गुंडों का नाड़ा खोल देते हैं।
हमारे भारत की फ़िल्म इंडस्ट्रीज बहुत सोच समझकर विलन का क़िरदार वर्गीकृत करती है। अब बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही ले लीजिए। अधिकतर बॉलीवुड फ़िल्म में विलन का एक ही ढर्रा हमेशा से रहा है। वो यह कि या तो ये साहब किसी 'भौकाली' सरदार के नीचे काम करते हैं या तो किसी शरीफ़ और मलूक बिजनेसमैन के बिज़नेस में हाथ बटाते हैं। फिर एकदिन मौका पाते ही अपने अन्नदाताओं को टपकाकर एक ही घिसा-पिटा डायलॉग बोलते हुए मिल जाते हैं कि 'इस दिन का मैंने बरसों इंतज़ार किया है, तब जाकर आज मेरा सपना पूरा हुआ।' अब इनसे कहो कि अबे उल्लू के दिमाग़! इतने दिनों किसी गैराज में भी काम करता तो आज उसका मालिक तू होता भाई! ख़ैर, जाने दीजिए। तिसपर हीरो, हीरो का तो क्या ही कहें, आज के दौर में अकेला ही पूरे देश को निपटाने की सामर्थ्य रखता है।
दूसरा सबसे मशहूर टॉलीवुड इंडस्ट्रीज का नंबर आता है साहब! यहाँ मेन विलन से एक पोस्ट नीचे वाले गुर्गे ने सांडनुमा शरीर और कोयला खदान की आग में भुने हुए भक्क काले टट्टू पाल रखे होते हैं। जिनके हाथों में भगवान परशुराम के फरशे, असुर सम्राट रावण की तलवार से लेकर नारियल छीलने वाले भारी-भरकम चाकू की मौज़ूदगी होती है। मेन विलन की भूमिका में प्रकाश राज, आशीष विद्यार्थी, प्रदीप रावत, रघुवरन, जगपति बाबू और सोनू सूद जैसे हेकड़ और चौखड़ पट्ठे सामने निकल कर आते हैं। ये फ़िल्मों में अधिकतर रंजिश को भुनाते और भूनते हुए मिल जाते हैं या फिर इनकी लड़की का प्रेम प्रसंग उस हीरो से होते हुए चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका होता है जो जाने-अनजाने उस 'विलन' के लिए 'विलन' का रोल ही प्ले करता है।
मार-कुटाई के सीन में जब हीरो इन टट्टुओं की कुटाई करता है, तब किसी के मुँह के आगे इनके जूते का सोल पंखे से भी तेज हवा फेंकने लगता है। हीरो के एक घूँसे में सात समंदर पार की सुखद यात्रा का अनुभव भी इन टट्टुओं को ही नसीब होता है। हीरो वह महान व्यक्ति है जो अपनी माँ समान मिट्टी से प्रेम न करने वाले चिलगोजों को नाक रगड़ते हुए भूमि वंदन करने की विधि सिखाने की हैसियत रखता है। मतलब! सौ-सौ गुंडे एक सूखे-पाखे धनुष जैसे हीरो का जब कुछ नहीं उखाड़ पाते तो सिक्स पैक एब्स वालों का कुछ भी बिगाड़ पाना नामुमकिन ही होता है।
एक और बात, जो इन सारी फिल्मों में दिलचस्प होती है, वो यह कि जितना ताक़तवर विलन, उतना ही ताक़तवर हीरो। हीरो भाईसाहब को विलन मोटी-मोटी लोहे की रॉड से कितना भी मार ले पर साहब टस से मस नहीं होते बल्कि आँखों से इशारा देते हैं कि 'लल्लू! तू तो गया काम से।' विलन की नापाक हरक़त का हासिल सिर्फ़ इतना होता है कि हीरो उठकर खड़ा हो जाता है जिसे देखते ही घंटों से हीरो की कुटाई कर रहे विलन को मिली थकान और बौखलाहट के मारे उसका चेहरा लाल-पीला हो जाता है। और यहाँ फिर कोई ग़लती होती है जिसके फलस्वरूप हीरो विलन को इतना लतियाता है कि जिसे देखकर भूत भी भाग जाए। अंत समय में विलन दुख भोगता हुआ नर्क के दरवाज़े पर अपनी नाक रगड़ता है और हीरो, अपनी हीरोइन या फिर फैमिली के साथ ख़ुश होते हुए फोटो खिंचा लेता है।
अब आते हैं लगभग तीन घंटे की फ़िल्म की असलियत पर। फ़िल्म ख़त्म होते ही दर्शकों का एक जत्था भक्तों की तरह खड़े होकर तालियाँ पीटता है जैसे रघुनाथ जी के दर्शन कर लिए हों और उनके आगे सिर झुका रहा हो। इसके अलावा थिएटर में बैठे आधे से ज़्यादा दर्शक दीर्घा में पड़े-पड़े ऊँघ रहे होते हैं। कभी-कभी कुछ एक दर्शक हीरो के मर जाने का ढेर सारा शोक मनाते हुए बाहर आते हैं और अपने दोस्तों की कमीज़ से ही नाक पोंछ कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे देते हैं। कभी मेरी पेशानी पर भी बल पड़ता था। सोचता था कि कैसे एक हीरो इतने गुंडों को मार लेता है? क्या हीरो इतना हैंडसम होता है? ये गुंडे काले-कूबरे और चौखटे जैसे मुँह के ही क्यों होते हैं? वगैरह, वगैरह। लेकिन जब बड़ा हुआ तो फ़िल्म देखते-देखते ही इन सब सवालों का जवाब भी मिल गया। फ़िलहाल, हम सबको अपने ज़ेहन में इस बात की गाँठ बाँधकर रखनी होगी कि मनोरंजन की दुनिया हक़ीक़त से कभी भी मेल नहीं खा सकती। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम अच्छाई को फिल्मों से निकालें और उन्हें आपने जीवन में आत्मसात करें। और हाँ! फ़िल्म देखने के दौरान नकारात्मकता और बनावटी पहलुओं को आग लगाकर मन के किसी भी कोने से दूर फेंक देना ही बेहतर होगा। अच्छा रहेगा कि हम तथ्यपरक और यथार्थ से जुड़ी फ़िल्मों को देखें। यह हमारे सुखद कल के लिए एकदम उपयुक्त चुनाव होगा वरना आने वाले परिणाम हमें अवश्य ही चिंतित करेंगे, जिस तरह से आज करते हैं।
-खेरवार

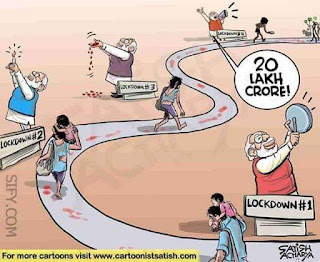


Comments
Post a Comment